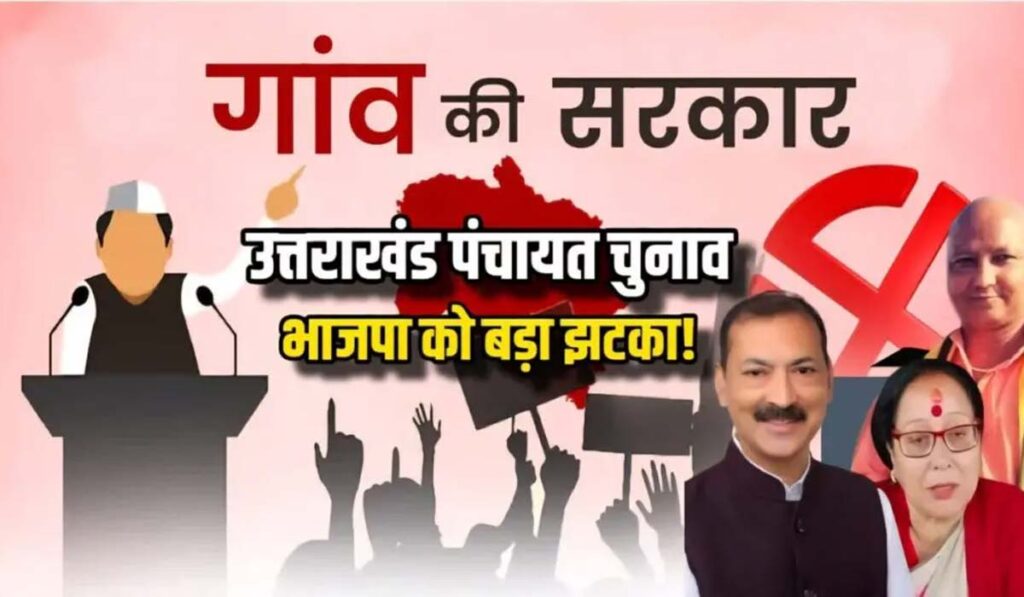
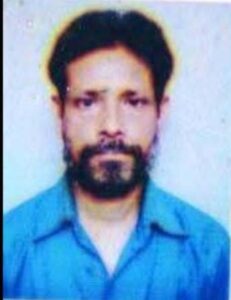
सलीम रज़ा (पत्रकार)
उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव 2025 में जिस तरह से समीकरण बदले हैं, वह न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर संकेत करता है। यह बदलाव केवल प्रत्याशियों के नामों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गांव की सत्ता संरचना, मतदाताओं की प्राथमिकताओं और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई यानी ‘पंचायत’ की परिभाषा तक को प्रभावित करता दिखा।
इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास रहा। जहां पहले स्थानीय चुनावों में वंशवाद, जातीय गठजोड़ और पारंपरिक समीकरणों का बोलबाला होता था, वहीं इस बार आमजन ने इन सभी को एक हद तक किनारे रखकर विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को तरजीह दी। उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से विकास की धीमी रफ्तार, पलायन की गंभीर समस्या और युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं अब पंचायत चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं।
एक महत्वपूर्ण कारण रहा – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए परिसीमन और आरक्षण से जुड़े बदलाव। जब किसी वार्ड या ग्राम पंचायत में सीट का आरक्षण बदलता है, तो वहां के वर्षों पुराने समीकरण स्वतः ही ध्वस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जहां कभी एक प्रभावशाली नेता का दबदबा था, वहां अब आरक्षण महिला, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कर दिया गया। इससे न केवल सत्ता संतुलन बदला, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि लोकतंत्र का लाभ हर वर्ग और लिंग तक पहुंचे।
इस आरक्षण नीति के चलते कई ऐसे नए चेहरे उभरे जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। खासकर महिलाओं ने बड़ी संख्या में मैदान में उतरकर न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि बड़ी जीत भी दर्ज की। यह एक सामाजिक बदलाव का संकेत है कि अब महिलाएं केवल आरक्षित सीटों की ‘प्रॉक्सी’ उम्मीदवार नहीं रहीं, बल्कि वे अपनी नीतियों, नेतृत्व क्षमता और जमीनी कार्यों के दम पर चुनाव जीत रही हैं। कई जगहों पर तो महिलाओं ने अपने पति, परिवार या राजनीतिक संरक्षण के बिना प्रचार किया और जनता से सीधे संवाद स्थापित कर चुनाव जीता।
युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। पढ़े-लिखे युवाओं ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि पंचायत में नई सोच और तकनीकी समझ लेकर आए। वे जानकार थे कि ग्राम पंचायत पोर्टल कैसे काम करता है, सरकारी योजनाएं कैसे लाई जाती हैं, ग्राम निधि का उपयोग किस तरह पारदर्शिता से किया जा सकता है। यह डिजिटल युग के लोकतंत्र का संकेत है – जहां गांव की राजनीति में भी अब ई-गवर्नेंस और आईटी की भूमिका बढ़ने लगी है।
पंचायत चुनावों में चुनाव प्रचार के तौर-तरीके भी बदले हैं। पहले जहां प्रचार-प्रसार का माध्यम केवल माइक और जनसभाएं हुआ करती थीं, वहीं अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, छोटे वीडियो क्लिप्स, डिजिटल बैनर और ऑनलाइन जनसंपर्क भी आम हो गया है। ग्रामीण युवाओं ने इसका उपयोग न केवल प्रचार के लिए किया, बल्कि पारदर्शिता और शिकायतों के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया।
इस पूरे चुनावी परिदृश्य में एक और बड़ा बदलाव यह दिखा कि मतदाता अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गया है। वह जानता है कि उसका वोट केवल परंपरा नहीं, बल्कि आने वाले पांच वर्षों का भविष्य तय करता है। यही कारण है कि मतदान प्रतिशत कई स्थानों पर बढ़ा, खासकर महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में उत्साह अधिक दिखा।
सत्ता का विकेंद्रीकरण – यानि सरकार का ग्राम स्तर तक पहुंचना – तब ही सफल हो सकता है जब स्थानीय प्रतिनिधि वास्तव में जनहित में काम करें और जनता उनके काम का मूल्यांकन कर सके। इस बार मतदाताओं ने इस कसौटी पर कई पुराने चेहरों को खारिज कर नए उम्मीदवारों को मौका दिया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है – कि इसमें बदलाव हमेशा संभव रहता है।
कई क्षेत्रों में यह भी देखा गया कि प्रत्याशियों ने केवल अपने वादों पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अपने पुराने कार्यों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। कुछ ने अपने खर्चों का ब्यौरा दिया, तो कुछ ने सोशल ऑडिट करवाई, जिससे मतदाताओं का विश्वास और बढ़ा।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यह बदलाव और भी अधिक गहराई से महसूस किया गया, जहां वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े थे, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, सड़कों की हालत खराब थी, पानी की आपूर्ति अनियमित थी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कमजोर थीं। इन मुद्दों को लेकर ग्रामीण मतदाता अब चुप नहीं हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सवाल करना शुरू कर दिया है – “किस योजना में कितना पैसा आया”, “कौन-सा काम कब हुआ”, “किसे लाभ मिला”, और “किसी को क्यों नहीं मिला” – ये प्रश्न अब आम हो गए हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव ने इस बार कई पुराने मिथकों को तोड़ा है। न तो अब जाति का जादू पहले जैसा है, न ही खानदानी नेताओं का असर। अब गांव की सरकार में वही आएगा जो जवाबदेह हो, जो पढ़ा-लिखा हो, जो तकनीक समझता हो, और सबसे जरूरी – जो गांव की मिट्टी से जुड़ा हो। यह परिवर्तन केवल वर्तमान चुनाव का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है, जो राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है।
यदि यह रुझान ऐसे ही बना रहा, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायतें न केवल छोटे विकास केंद्र बनेंगी, बल्कि राज्य के सुशासन की मजबूत बुनियाद भी बन सकती हैं। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि चेतना का है — और चेतना जब जागती है, तो बदलाव रुकता नहीं है।








